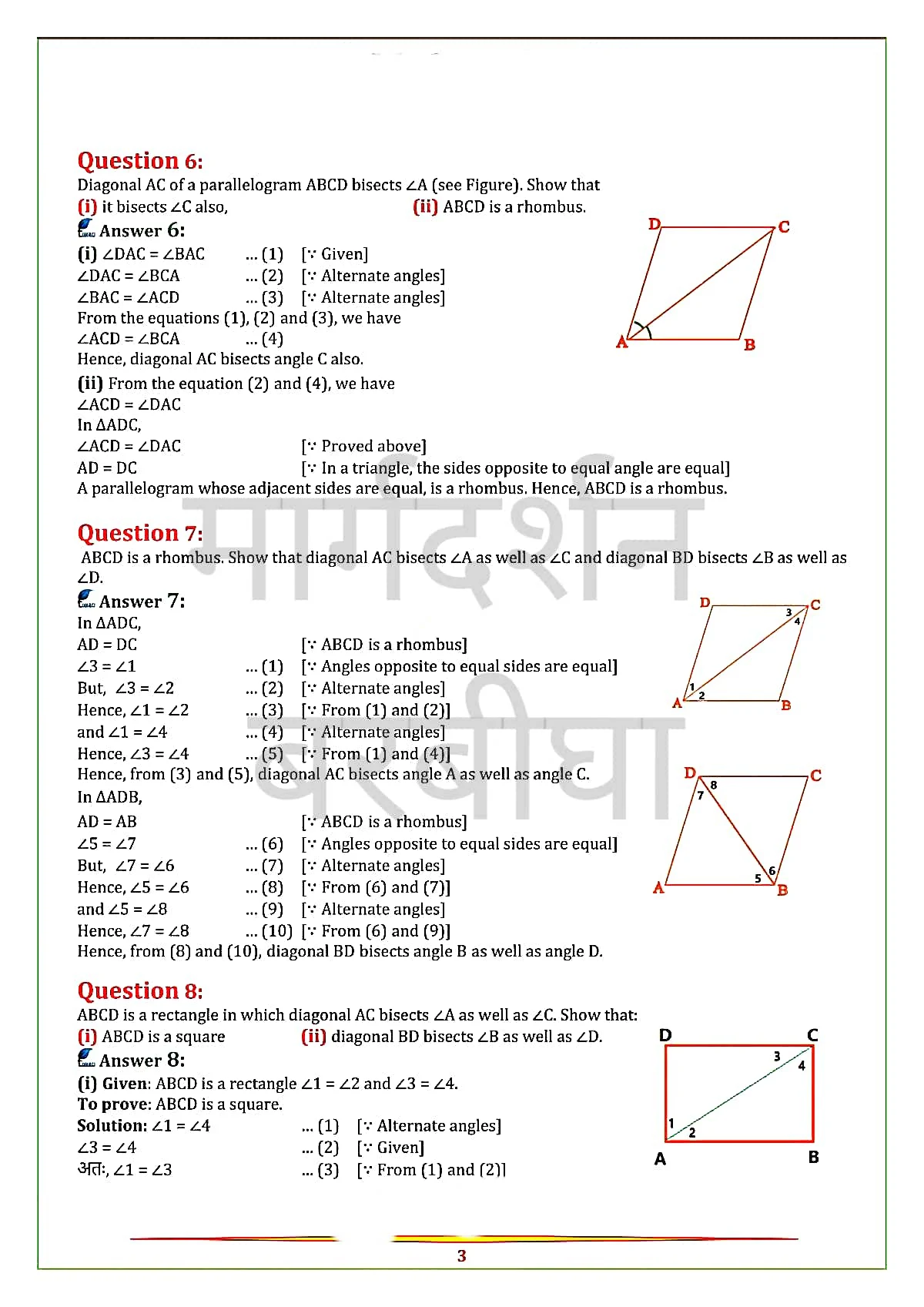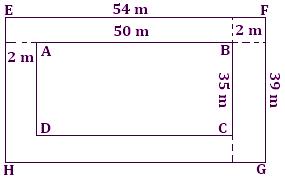पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है जो इस प्रकार है।
1 परिवार और मित्र(Family and friends)
2 भोजन(Food)
3 आश्रय( shelter)
4 पानी( water)
5 यात्रा( travel)
6 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं (Things we make and do)
पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005(NCF 2005) बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है।
- पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं ,बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है।
- पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है । यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है।
- पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द “इंवीरोनर”से लिया गया है जिसका अर्थ है पूरा परिवेश।
1 पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन चक्रवात आंधी के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं।
2 इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं।
3 प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है।
4 पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में ना सिर्फ पृथ्वी वरन अंतरिक्ष भी सम्मिलित है
5 मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं ।
6 मौसम संबंधी अनेक कारण जैसे कि तापमान,, पवन, दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात ,पाला पड़ना भी पर्यावरण के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रगट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उनके निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं ।
7 पर्यावरण का क्षेत्र काफी व्यापक होता है पर्यावरण अध्ययन को 3:00 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है।
- पर्यावरण के बारे में सीखना।
- पर्यावरण के लिए सीखना।
- पर्यावरण के माध्यम से सीखना।
8 पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर, इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है इस की विषय वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती है ।
9 पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझा ना ही नहीं बल्कि-
- सकारात्मक अभिवृत्तियो , मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के महत्व को समझने का विकास भी करना है।
- पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना।
- संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाना ।
पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन(Significance of Evs ,Integrated Evs)
- पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा (Science, social science, Environmental education) की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि तैयार की जाती है।
- प्रत्येक विषय के शिक्षण का अपना उद्देश्य है अपना महत्व है एवं इससे विषय के सीखने की प्रक्रिया जुड़ी है।
पर्यावरण अध्ययन का महत्व Significance of Evs
1 संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है, यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मार कर पढ़ने से नहीं होता बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है।
2 पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है। बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराया जाए पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रति देश की छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं।
3 हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है, कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है, तथा इसका महत्व क्या है पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है।
4 पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं।
5 पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं।
6 पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य की बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके।
7 यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है।
8 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है।
9 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है।
10 पर्यावरण अध्ययन NCF 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है, पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना।
11 इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं।
12 इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने के कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, जैसे की दल के साथ काम करना, उनकी बात सुनना तथा उनसे बात करना सीखना आदि।
13 इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है। विचारों, अनुभवों लोगो, भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक-सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सीखते हैं।
14 अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं ।
15 अधिगम इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के द्वारा संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद काम करना, प्रश्न करना सुनना तथा सहक्रिय करना मुख्य क्रियाए हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है, पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक है ।
एकीकृत पर्यावरण अध्ययन(Integrated Evs)
1 हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा( 1975, 1988, 2000, 2005) इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में” पर्यावरण के बचाव” को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात कही गई है अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
3 राष्ट्रीय स्तर पर N.C.E. R.T द्वारा विकसित सब्जी पाठ्यचर्या में इस पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया है।
4 1975 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या(NCF 1975) प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की थी। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 और कक्षा दो में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए एवं कक्षा 3 व 4 तक इसमें दो विषय के रूप में अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन 1 ( प्राकृतिक विज्ञान) और पर्यावरण अध्ययन 2 ( सामाजिक विज्ञान) पढ़ाया जाना चाहिए ।
5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988(NCF 1988) में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को ही मंजूर किया गया था।
बोझ रहित अधिगम ( शिक्षा: राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993)
ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977,NCERT कार्य समूह( 1984) और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति(1990) ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशें की लेकिन कम होने के बजाय समस्या और अधिक तीव्र हो गई ,और इसीलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की( भारत सरकार 1993)
इसके उद्देश्यों में शामिल है-” जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रोंप् पर भार को कम करने के लिए तरीके और साधन सूझाना”
इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की( 1993) “ बोझ रहित शिक्षण” – पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्णय को काफी हद तक इसके द्वारा निर्देशित किया गया था।
NCF -2000 (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000)
NCF -2000 ने पहली बार सुझाव दिया की विभिन्न विषयों के विचारों और अवधारणाओं को एकीकृत किया जाए । जैसे- भारत की संस्कृति विरासत पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानूनी साक्षरता, मानव अधिकार शिक्षा, वैज्ञानिक सोच का पोषण इत्यादि।
NCF -2000 मैं पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में प्रथक प्रथक ना कर एकीकृत रूप में पढ़ने की सिफारिश की गई थी इसके अनुसार-
- कक्षा 1 व 2 ने इसे पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं रख कर इसे भाषा और गणित विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया गणित की सामग्री बच्चे के नजदीक पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी है।
- कक्षा 3 व 4 में बच्चों को पर्यावरण एवं उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त ना करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया।
NCF -2005 (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005)
- NCF -2005 मैं भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक रत रूप में ही सशक्त रूप से पढ़ने पर बल दिया गया।
- कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण संबंधी कौशल एवं सरोकारों को भाषा एवं गणित के माध्यम से संबोधित करने की संस्तुति दी गई।
- कक्षा 3 बा 4 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति दी गई।
पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता-
ऐसा माना जाता है, कि बच्चा टुकड़े टुकड़े में खंडित बातों की बजाय संपूर्णता मैं बातों को आसानी से समझता है। जैसे कि बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है। वह पेड़ को घर का पेड़ या बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है। वह मूर्त बातों को ही देखता हैऐसे में हम यदि उसे अमूर्त और अनुभव से परे की बात बताने लगे तो वह उन्हें अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाएगा और सूचनाओं को रटने लगेगा अपनी पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएगा।
NCERT द्वारा कक्षा 3- 5: तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत, स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्रों की पहचान की जिसमें बहु विशेयकता को एकीकृत किया गया इन्हें ”थीम” अर्थात प्रकरण कहां गया।
- परिवार एवं मित्र( संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल)
- भोजन
- आश्रय\ आवाज
- पानी
- यात्रा
- चीजें जो हम बनाते और करते हैं
1 “परिवार एवं मित्र” प्रकरण की भाग के रूप में
- “पौधे” एवं” जानवर” : “पौधे” एवं” जानवर परिवार एवं मित्र प्रकरण में सोच समझकर शामिल किए गए हैं । यह स्पष्ट करने के लिए कि मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं तथा हमें उनके बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है।
- “रिश्ते\ संबंध” : इस उपप्रकरण में, वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं और जो कहीं और चले गए हैं जिससे उनके रिश्ते और घरों में क्या बदलाव आए हैं। उसका ज्ञान मिलता है वह सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों में कौन-कौन प्रशंसा के पात्र हैं एवं किन किन गुणों या कौशलों के कारण संबंध तथा परिवारों से बच्चों में अपनेपन तथा प्रेम की भावना का विकास होता है।
- “ काम तथा खेल” : इस उपप्रकरण से उन्हें यह पता चलता है, कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेज दो पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है।
- वे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलता है किस प्रकार पारंपरिक खेल तथा खिलौने से वह अलग है यह समझ मिलती है।
Environmental studies and environmental education (पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा)
पर्यावरण अध्ययन(EVS) (Environmental studies)
पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। अतः जब हम अपने परिवेश, अर्थात इर्द-गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और बौद्धिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पर्यावरण अध्ययन कहलाता है।
सामाजिक घटक- भाषा, मूल्य, संस्कृति
भौतिक घटक- वनस्पति, पशु पक्षी, हवा, पानी
पर्यावरण शिक्षा(environmental education)
पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए परिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए?
अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों इसके घटकों एवं मानव के साथ अंतः संबंध है । परिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव आदि की समुचित जानकारी देना। .
उद्देश्य-
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान कराने के साथ साथ जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के आवश्यक कौशल को प्रदान करना है।
आज के बच्चे आंतरिक खेलों और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को खेलने में व्यस्त रहते हैं। जिससे उन्हें अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने के अवसर नहीं मिलते छात्रों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसलिए पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है।
पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य(NCF 2005) Objectives of environmental studies)
- बच्चों का उनके वास्तविक संसार( प्राकृतिक एवं सामाजिक- सांस्कृतिक) से परिचित करवाना, पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करना।
- प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास कराना।
- पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता कराना।
- पर्यावरण के अनुकूल मनोवृति ओ तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषितकरना।
- अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना।
- पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें कि अतीत से अब में पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है।
- पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक होना।
- पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना।
- प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उनका स्तर देने के लिए परिकल्पना(Hypothese) बनाने की क्षमता का विकास कराना।
- परिकल्पना ओं की जांच के तरीके सोच पानी एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना।
- निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना।
- बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले।
- भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।